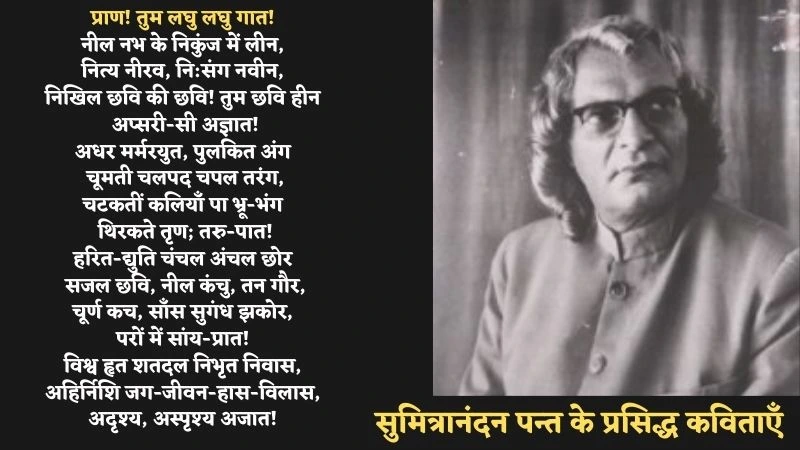
Sumitranandan Pant Poems in Hindi : आज यहाँ इस लेख में आपको सुमित्रानंदन पन्त के प्रसिद्ध कवितायेँ उपलब्ध करायेंगे अक्सर छात्रो को पढाई के दौरान या परीक्षा के दौरान Sumitranandan Pant Poems लिखने को मिलता है,
भारत के प्रसिद्ध कवियों के सूची सुमित्रानंदन पन्त जी का नाम देखने को मिलता है इनके द्वारा लिखे गये कविता हमें अक्सर हिंदी के पुस्तकों में देखने को मिलता है।
सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म बागेश्वर ज़िले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ई॰ को हुआ था जन्म के छह घंटे बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया उनका लालन-पालन उनकी दादी ने किया।
सात वर्ष की उम्र में, जब वे चौथी कक्षा में ही पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरु कर दिया था इनके द्वारा लिखे गये कविता काफी प्रसिद्ध होते है सुमित्रानंदन पन्त के कई सारे प्रसिद्ध कवितायेँ मौजूद है जो अक्सर हमें किताबो में देखने को मिलते है यहाँ आपको Sumitranandan Pant Poems in Hindi जारी किये है।
महात्मा जी के प्रति – सुमित्रानंदन पंत (1)
निर्वाणोन्मुख आदर्शों के अंतिम दीप शिखोदय!–
जिनकी ज्योति छटा के क्षण से प्लावित आज दिगंचल,–
गत आदर्शों का अभिभव ही मानव आत्मा की जय,
अत: पराजय आज तुम्हारी जय से चिर लोकोज्वल!
मानव आत्मा के प्रतीक! आदर्शों से तुम ऊपर,
निज उद्देश्यों से महान, निज यश से विशद, चिरंतन;
सिद्ध नहीं, तुम लोक सिद्धि के साधक बने महत्तर,
विजित आज तुम नर वरेण्य, गणजन विजयी साधारण!
युग युग की संस्कृतियों का चुन तुमने सार सनातन
नव संस्कृति का शिलान्यास करना चाहा भव शुभकर
साम्राज्यों ने ठुकरा दिया युगों का वैभव पाहन–
पदाघात से मोह मुक्त हो गया आज जन अन्तर!
दलित देश के दुर्दम नेता, हे ध्रुव, धीर, धुरंधर,
आत्म शक्ति से दिया जाति शव को तुमने जीवन बल;
विश्व सभ्यता का होना था नखशिख नव रूपांतर,
राम राज्य का स्वप्न तुम्हारा हुआ न यों ही निष्फल!
विकसित व्यक्तिवाद के मूल्यों का विनाश था निश्चय,
वृद्ध विश्व सामंत काल का था केवल जड़ खँडहर!
हे भारत के हृदय! तुम्हारे साथ आज नि:संशय
चूर्ण हो गया विगत सांस्कृतिक हृदय जगत का जर्जर!
गत संस्कृतियों का आदर्शों का था नियत पराभव,
वर्ग व्यक्ति की आत्मा पर थे सौध धाम, जिनके स्थित;
तोड़ युगों के स्वर्ण पाश अब मुक्त हो रहा मानव,
जन मानवता की भव संस्कृति आज हो रही निर्मित!
किए प्रयोग नीति सत्यों के तुमने जन जीवन पर,
भावादर्श न सिद्ध कर सके सामूहिक-जीवन-हित;
अधोमूल अश्वत्थ विश्व, शाखाएँ संस्कृतियाँ वर,
वस्तु विभव पर ही जनगण का भाव विभव अवलंबित!
वस्तु सत्य का करते भी तुम जग में यदि आवाहन,
सब से पहले विमुख तुम्हारे होता निर्धन भारत;
मध्य युगों की नैतिकता में पोषित शोषित-जनगण
बिना भाव-स्वप्नों को परखे कब हो सकते जाग्रत?
सफल तुम्हारा सत्यान्वेषण, मानव सत्यान्वेषक!
धर्म, नीति के मान अचिर सब, अचिर शास्त्र, दर्शन मत,
शासन जन गण तंत्र अचिर-युग स्थितियाँ जिनकी प्रेषक,
मानव गुण, भव रूप नाम होते परिवर्तित युगपत!
पूर्ण पुरुष, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अहिंसक,
मुक्त-हुए-तुम-मुक्त-हुए-जन, हे जग वंद्य महात्मन्!
देख रहे मानव भविष्य तुम मनश्चक्षु बन अपलक,
धन्य, तुम्हारे श्री चरणों से धरा आज चिर पावन!
बापू के प्रति – सुमित्रानंदन पंत (2)
तुम मांस-हीन, तुम रक्त-हीन,
हे अस्थि-शेष! तुम अस्थि-हीन,
तुम शुद्ध-बुद्ध आत्मा केवल,
हे चिर पुराण, हे चिर नवीन
तुम पूर्ण इकाई जीवन की,
जिसमें असार भव-शून्य लीन;
आधार अमर, होगी जिसपर
भावी की संस्कृति समासीन!
तुम मांस, तुम्ही हो रक्त-अस्थि,–
निर्मित जिनसे नवयुग का तन,
तुम धन्य! तुम्हारा नि:स्व-त्याग
है विश्व-भोग का वर साधन।
इस भस्म-काम तन की रज से
जग पूर्ण-काम नव जग-जीवन
बीनेगा सत्य-अहिंसा के
ताने-बानों से मानवपन!
सदियों का दैन्य-तिमिर तूम,
धुन तुमने कात प्रकाश-सूत,
हे नग्न! नग्न-पशुता ढँक दी
बुन नव संस्कृत मनुजत्व पूत।
जग पीड़ित छूतों से प्रभूत,
छू अमित स्पर्श से, हे अछूत!
तुमने पावन कर, मुक्त किये
मृत संस्कृतियों के विकृत भूत!
सुख-भोग खोजने आते सब,
आये तुम करने सत्य खोज,
जग की मिट्टी के पुतले जन,
तुम आत्मा के, मन के मनोज!
जड़ता, हिंसा, स्पर्धा में भर
चेतना, अहिंसा, नम्र-ओज,
पशुता का पंकज बना दिया
तुमने मानवता का सरोज!
पशु-बल की कारा से जग को
दिखलाई आत्मा की विमुक्ति,
विद्वेष, घृणा से लड़ने को
सिखलाई दुर्जय प्रेम-युक्ति;
वर श्रम-प्रसूति से की कृतार्थ
तुमने विचार-परिणीत उक्ति,
विश्वानुरक्त हे अनासक्त!
सर्वस्व-त्याग को बना भुक्ति!
सहयोग सिखा शासित-जन को
शासन का दुर्वह हरा भार,
होकर निरस्त्र, सत्याग्रह से
रोका मिथ्या का बल-प्रहार:
बहु भेद-विग्रहों में खोई
ली जीर्ण जाति क्षय से उबार,
तुमने प्रकाश को कह प्रकाश,
औ अन्धकार को अन्धकार।
उर के चरखे में कात सूक्ष्म
युग-युग का विषय-जनित विषाद,
गुंजित कर दिया गगन जग का
भर तुमने आत्मा का निनाद।
रँग-रँग खद्दर के सूत्रों में
नव-जीवन-आशा, स्पृह्यालाद,
मानवी-कला के सूत्रधार!
हर लिया यन्त्र-कौशल-प्रवाद।
जड़वाद जर्जरित जग में तुम
अवतरित हुए आत्मा महान,
यन्त्राभिभूत जग में करने
मानव-जीवन का परित्राण;
बहु छाया-बिम्बों में खोया
पाने व्यक्तित्व प्रकाशवान,
फिर रक्त-माँस प्रतिमाओं में
फूँकने सत्य से अमर प्राण!
संसार छोड़ कर ग्रहण किया
नर-जीवन का परमार्थ-सार,
अपवाद बने, मानवता के
ध्रुव नियमों का करने प्रचार;
हो सार्वजनिकता जयी, अजित!
तुमने निजत्व निज दिया हार,
लौकिकता को जीवित रखने
तुम हुए अलौकिक, हे उदार!
मंगल-शशि-लोलुप मानव थ
विस्मित ब्रह्मांड-परिधि विलोक
तुम केन्द्र खोजने आये त
सब में व्यापक, गत राग-शोक;
पशु-पक्षी-पुष्पों से प्रेरित
उद्दाम-काम जन-क्रान्ति रोक,
जीवन-इच्छा को आत्मा के
वश में रख, शासित किए लोक।
था व्याप्त दिशावधि ध्वान्त भ्रान्त
इतिहास विश्व-उद्भव प्रमाण,
बहु-हेतु, बुद्धि, जड़ वस्तु-वाद
मानव-संस्कृति के बने प्राण;
थे राष्ट्र, अर्थ, जन, साम्य-वा
छल सभ्य-जगत के शिष्ट-मान,
भू पर रहते थे मनुज नहीं,
बहु रूढि-रीति प्रेतों-समान–
तुम विश्व मंच पर हुए उदित
बन जग-जीवन के सूत्रधार,
पट पर पट उठा दिए मन से
कर नव चरित्र का नवोद्धार;
आत्मा को विषयाधार बना,
दिशि-पल के दृश्यों को सँवार,
गा-गा–एकोहं बहु स्याम,
हर लिए भेद, भव-भीति-भार!
एकता इष्ट निर्देश किया,
जग खोज रहा था जब समता,
अन्तर-शासन चिर राम-राज्य,
औ’ बाह्य, आत्महन-अक्षमता;
हों कर्म-निरत जन, राग-विरत
रति-विरति-व्यतिक्रम भ्रम-ममता,
प्रतिक्रिया-क्रिया साधन-अवयव,
है सत्य सिद्ध, गति-यति-क्षमता।
ये राज्य, प्रजा, जन, साम्य-तन्त्र
शासन-चालन के कृतक यान,
मानस, मानुषी, विकास-शास्त्र
हैं तुलनात्मक, सापेक्ष ज्ञान;
भौतिक विज्ञानों की प्रसूति
जीवन-उपकरण-चयन-प्रधान,
मथ सूक्ष्म-स्थूल जग, बोले तुम–
मानव मानवता का विधान!
साम्राज्यवाद था कंस, बन्दिनी
मानवता पशु-बलाक्रान्त,
शृंखला दासता, प्रहरी बहु
निर्मम शासन-पद शक्ति-भ्रान्त;
कारा-गृह में दे दिव्य जन्म
मानव-आत्मा को मुक्त, कान्त,
जन-शोषण की बढ़ती यमुना
तुमने की नत-पद-प्रणत, शान्त!
कारा थी संस्कृति विगत, भित्ति
बहु धर्म-जाति-गत रूप-नाम,
बन्दी जग-जीवन, भू-विभक्त,
विज्ञान-मूढ़ जन प्रकृति-काम;
आए तुम मुक्त पुरुष, कहने–
मिथ्या जड़-बन्धन, सत्य राम,
नानृतं जयति सत्यं, मा भैः
जय ज्ञान-ज्योति, तुमको प्रणाम!
अनुभूति – सुमित्रानंदन पंत (3)
तुम आती हो,
नव अंगों का
शाश्वत मधु-विभव लुटाती हो।
बजते नि:स्वर नूपुर छम-छम,
सांसों में थमता स्पंदन-क्रम,
तुम आती हो,
अंत:स्थल में
शोभा ज्वाला लिपटाती हो।
अपलक रह जाते मनोनयन
कह पाते मर्म-कथा न वचन,
तुम आती हो,
तंद्रिल मन में,
स्वप्नों के मुकुल खिलाती हो।
अभिमान अश्रु बनता झर-झर,
अवसाद मुखर रस का निर्झर,
तुम आती हो,
आनंद-शिखर,
प्राणों में ज्वार उठाती हो।
स्वर्णिम प्रकाश में गलता तम,
स्वर्गिक प्रतीति में ढलता श्रम
तुम आती हो,
जीवन-पथ पर,
सौंदर्य-रस बरसाती हो।
जगता छाया-वन में मर्मर,
कंप उठती रुद्ध स्पृहा थर-थर,
तुम आती हो,
उर तंत्री में,
स्वर मधुर व्यथा भर जाती हो।
मोह -सुमित्रानंदन पंत (4)
छोड़ द्रुमों की मृदु-छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले! तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन?
भूल अभी से इस जग को!
तज कर तरल-तरंगों को,
इन्द्र-धनुष के रंगों को,
तेरे भ्रू-भंगों से कैसे बिंधवा दूँ निज मृग-सा मन?
भूल अभी से इस जग को!
कोयल का वह कोमल-बोल,
मधुकर की वीणा अनमोल,
कह, तब तेरे ही प्रिय-स्वर से कैसे भर लूँ सजनि! श्रवन?
भूल अभी से इस जग को!
ऊषा-सस्मित किसलय-दल,
सुधा रश्मि से उतरा जल,
ना, अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूँ जीवन?
भूल अभी से इस जग को
सांध्य वंदना – सुमित्रानंदन पंत (5)
जीवन का श्रम ताप हरो हे!
सुख सुषुमा के मधुर स्वर्ण हे!
सूने जग गृह द्वार भरो हे!
लौटे गृह सब श्रान्त चराचर
नीरव, तरु अधरों पर मर्मर,
करुणानत निज कर पल्लव से
विश्व नीड प्रच्छाय करो हे!
उदित शुक्र अब, अस्त भनु बल,
स्तब्ध पवन, नत नयन पद्म दल
तन्द्रिल पलकों में, निशि के शशि!
सुखद स्वप्न वन कर विचरो हे!
वायु के प्रति – सुमित्रानंदन पंत (6)
प्राण! तुम लघु लघु गात!
नील नभ के निकुंज में लीन,
नित्य नीरव, नि:संग नवीन,
निखिल छवि की छवि! तुम छवि हीन
अप्सरी-सी अज्ञात!
अधर मर्मरयुत, पुलकित अंग
चूमती चलपद चपल तरंग,
चटकतीं कलियाँ पा भ्रू-भंग
थिरकते तृण; तरु-पात!
हरित-द्युति चंचल अंचल छोर
सजल छवि, नील कंचु, तन गौर,
चूर्ण कच, साँस सुगंध झकोर,
परों में सांय-प्रात!
विश्व हृत शतदल निभृत निवास,
अहिर्निशि जग-जीवन-हास-विलास,
अदृश्य, अस्पृश्य अजात!
श्री सूर्यकांत त्रिपाठी के प्रति – सुमित्रानंदन पंत (7)
छंद बंध ध्रुव तोड़, फोड़ कर पर्वत कारा
अचल रूढ़ियों की, कवि! तेरी कविता धारा
मुक्त अबाध अमंद रजत निर्झर-सी नि:सृत–
गलित ललित आलोक राशि, चिर अकलुष अविजित!
स्फटिक शिलाओं से तूने वाणी का मंदिर
शिल्पि, बनाया — ज्योति कलश निज यश का घर चित्त।
शिलीभूत सौन्दर्य ज्ञान आनंद अनश्वर
शब्द-शब्द में तेरे उज्ज्वल जड़ित हिम शिखर।
शुभ्र कल्पना की उड़ान, भव भास्वर कलरव,
हंस, अंश वाणी के, तेरी प्रतिभा नित नव;
जीवन के कर्दम से अमलिन मानस सरसिज
शोभित तेरा, वरद शारदा का आसन निज।
अमृत पुत्र कवि, यशकाय तव जरा-मरणजित,
स्वयं भारती से तेरी हृतंत्री झंकृत।
आज रहने दो यह गृह-काज – सुमित्रानंदन पंत (8)
आज रहने दो यह गृह-काज,
प्राण! रहने दो यह गृह-काज!
आज जाने कैसी वातास,
छोड़ती सौरभ-श्लथ उच्छ्वास,
प्रिये लालस-सालस वातास,
जगा रोओं में सौ अभिलाष।
आज उर के स्तर-स्तर में, प्राण!
सजग सौ-सौ स्मृतियाँ सुकुमार,
दृगों में मधुर स्वप्न-संसार,
मर्म में मदिर-स्पृहा का भार!
शिथिल, स्वप्निल पंखड़ियाँ खोल,
आज अपलक कलिकाएँ बाल,
गूँजता भूला भौंरा डोल,
सुमुखि! उर के सुख से वाचाल!
आज चंचल-चंचल मन-प्राण,
आज रे शिथिल-शिथिल तन भार;
आज दो प्राणों का दिन-मान,
आज संसार नहीं संसार!
आज क्या प्रिये, सुहाती लाज?आज रहने दो सब गृह-काज!
चंचल पग दीप-शिखा-से – सुमित्रानंदन पंत (9)
चंचल पग दीप-शिखा-से धर
गृह,मग, वन में आया वसन्त!
सुलगा फाल्गुन का सूनापन
सौन्दर्य-शिखाओं में अनन्त!
सौरभ की शीतल ज्वाला से
फैला उर-उर में मधुर दाह
आया वसन्त, भर पृथ्वी पर
स्वर्गिक सुन्दरता का प्रवाह!
पल्लव-पल्लव में नवल रुधिर
पत्रों में मांसल-रंग खिला,
आया नीली-पीली लौ से
पुष्पों के चित्रित दीप जला!
अधरों की लाली से चुपके
कोमल गुलाब के गाल लजा,
आया, पंखड़ियों को काले–
पीले धब्बों से सहज सजा!
कलि के पलकों में मिलन-स्वप्न,
अलि के अन्तर में प्रणय-गान
लेकर आया, प्रेमी वसन्त,–
आकुल जड़-चेतन स्नेह-प्राण!
काली कोकिल!–सुलगा उर में
स्वरमयी वेदना का अँगार,
आया वसन्त, घोषित दिगन्त
करती भव पावक की पुकार!
आः, प्रिये! निखिल ये रूप-रंग
रिल-मिल अन्तर में स्वर अनन्त
रचते सजीव जो प्रणय-मूर्ति
उसकी छाया, आया वसन्त!
संध्या के बाद – सुमित्रानंदन पंत (10)
सिमटा पंख साँझ की लाली
जा बैठी तरू अब शिखरों पर
ताम्रपर्ण पीपल से, शतमुख
झरते चंचल स्वर्णिम निझर!
ज्योति स्तंभ-सा धँस सरिता में
सूर्य क्षितिज पर होता ओझल
बृहद जिह्म ओझल केंचुल-सा
लगता चितकबरा गंगाजल!
धूपछाँह के रंग की रेती
अनिल ऊर्मियों से सर्पांकित
नील लहरियों में लोरित
पीला जल रजत जलद से बिंबित!
सिकता, सलिल, समीर सदा से,
स्नेह पाश में बँधे समुज्ज्वल,
अनिल पिघलकर सलिल, सलिल
ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल!
शंख घट बज गया मंदिर में
लहरों में होता कंपन,
दीप शीखा-सा ज्वलित कलश
नभ में उठकर करता निराजन!
तट पर बगुलों-सी वृद्धाएँ
विधवाएँ जप ध्यान में मगन,
मंथर धारा में बहता
जिनका अदृश्य, गति अंतर-रोदन!
दूर तमस रेखाओं सी,
उड़ती पंखों सी-गति चित्रित
सोन खगों की पाँति
आर्द्र ध्वनि से निरव नभ करती मुखरित!
स्वर्ण चूर्ण-सी उड़ती गोरज
किरणों की बादल-सी जलकर,
सनन तीर-सा जाता नभ में
ज्योतित पंखों कंठों का स्वर!
लौटे खग, गायें घर लौटीं
लौटे कृषक श्रांत श्लथ डग धर
छिपे गृह में म्लान चराचर
छाया भी हो गई अगोचर!
लौट पैंठ से व्यापारी भी
जाते घर, उस पार नाव पर,
ऊँटों, घोड़ों के संग बैठे
ख़ाली बोरों पर, हुक्का भर!
जोड़ों की सुनी द्वभा में,
झूल रही निशि छाया छाया गहरी,
डूब रहे निष्प्रभ विषाद में
खेत, बाग, गृह, तरू, तट लहरी!
बिरहा गाते गाड़ी वाले,
भूँक-भूँकर लड़ते कूकर,
हुआँ-हुआँ करते सियार,
देते विषण्ण निशि बेला को स्वर!
माली की मँड़इ से उठ,
नभ के नीचे नभ-सी धूमाली
मंद पवन में तिरती
नीली रेशम की-सी हलकी जाली!
बत्ती जल दुकानों में
बैठे सब कस्बे के व्यापारी,
मौन मंद आभा में
हिम की ऊँध रही लंबी अधियारी!
धुआँ अधिक देती है
टिन की ढबरी, कम करती उजियाली,
मन से कढ़ अवसाद श्रांति
आँखों के आगे बुनती जाला!
छोटी-सी बस्ती के भीतर
लेन-देन के थोथे सपने
दीपक के मंडल में मिलकर
मँडराते घिर सुख-दुख अपने!
कँप-कँप उठते लौ के संग
कातर उर क्रंदन, मूक निराशा,
क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों
गोपन मन को दे दी हो भाषा!
लीन हो गई क्षण में बस्ती,
मिली खपरे के घर आँगन,
भूल गए लाला अपनी सुधी,
भूल गया सब ब्याज, मूलधन!
सकूची-सी परचून किराने की ढेरी
लग रही ही तुच्छतर,
इस नीरव प्रदोष में आकुल
उमड़ रहा अंतर जग बाहर!
अनुभव करता लाला का मन,
छोटी हस्ती का सस्तापन,
जाग उठा उसमें मानव,
औ असफल जीवन का उत्पीड़न!
दैन्य दुख अपमान ग्लानि
चिर क्षुधित पिपासा, मृत अभिलाषा,
बिना आय की क्लांति बनी रही
उसके जीवन की परिभाषा
जड़ अनाज के ढेर सदृश ही
वह दीन-भर बैठा गद्दी पर
बात-बात पर झूठ बोलता
कौड़ी-सी स्पर्धा में मर-मर!
फिर भी क्या कुटुंब पलता है?
रहते स्वच्छ सुधर सब परिजन?
बना पा रहा वह पक्का घर?
मन में सुख है? जुटता है धन?
खिसक गई कंधों में कथड़ी
ठिठुर रहा अब सर्दी से तन,
सोच रहा बस्ती का बनिया
घोर विवशता का कारण!
शहरी बनियों-सा वह भी उठ
क्यों बन जाता नहीं महाजन?
रोक दिए हैं किसने उसकी
जीवन उन्नति के सब साधन?
यह क्यों संभव नहीं
व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन?
कर्म और गुण के समान ही
सकल आय-व्यय का हो वितरण?
घुसे घरौंदे में मिट्टी के
अपनी-अपनी सोच रहे जन,
क्या ऐसा कुछ नहीं,
फूँक दे जो सबमें सामूहिक जीवन?
मिलकर जन निर्माण करे जग,
मिलकर भोग जीवन करे जीवन का,
जन विमुक्त हो जन-शोषण से,
हो समाज अधिकारी धन का?
दरिद्रता पापों की जननी,
मिटे जनों के पाप, ताप, भय,
सुंदर हो अधिवास, वसन, तन,
पशु पर मानव की हो जय?
वक्ति नहीं, जग की परिपाटी
दोषी जन के दु:ख क्लेश की
जन का श्रम जन में बँट जाए,
प्रजा सुखी हो देश देश की!
टूट गया वह स्वप्न वणिक का,
आई जब बुढि़या बेचारी,
आध-पाव आटा लेने
लो, लाला ने फिर डंडी मारी!
चीख उठा घुघ्घू डालों में
लोगों ने पट दिए द्वार पर,
निगल रहा बस्ती को धीरे,
गाढ़ अलस निद्रा का अजगर!
वे आँखें – सुमित्रानंदन पंत (11)
अंधकार की गुहा सरीखी
उन आँखों से डरता है मन,
भरा दूर तक उनमें दारुण
दैन्य दुख का नीरव रोदन!
अह, अथाह नैराश्य, विवशता का
उनमें भीषण सूनापन,
मानव के पाशव पीड़न का
देतीं वे निर्मम विज्ञापन!
फूट रहा उनसे गहरा आतंक,
क्षोभ, शोषण, संशय, भ्रम,
डूब कालिमा में उनकी
कँपता मन, उनमें मरघट का तम!
ग्रस लेती दर्शक को वह
दुर्ज्ञेय, दया की भूखी चितवन,
झूल रहा उस छाया-पट में
युग युग का जर्जर जन जीवन!
वह स्वाधीन किसान रहा,
अभिमान भरा आँखों में इसका,
छोड़ उसे मँझधार आज
संसार कगार सदृश बह खिसका!
लहराते वे खेत दृगों में
हुया बेदख़ल वह अब जिनसे,
हँसती थी उनके जीवन की
हरियाली जिनके तृन तृन से!
आँखों ही में घूमा करता
वह उसकी आँखों का तारा,
कारकुनों की लाठी से जो
गया जवानी ही में मारा!
बिका दिया घर द्वार,
महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी,
रह रह आँखों में चुभती वह
कुर्क हुई बरधों की जोड़ी!
उजरी उसके सिवा किसे कब
पास दुहाने आने देती?
अह, आँखों में नाचा करती
उजड़ गई जो सुख की खेती!
बिना दवा दर्पन के घरनी
स्वरग चली,–आँखें आतीं भर,
देख रेख के बिना दुधमुँही
बिटिया दो दिन बाद गई मर!
घर में विधवा रही पतोहू,
लछमी थी, यद्यपि पति घातिन,
पकड़ मँगाया कोतवाल ने,
डूब कुँए में मरी एक दिन!
ख़ैर, पैर की जूती, जोरू
न सही एक, दूसरी आती,
पर जवान लड़के की सुध कर
साँप लोटते, फटती छाती!
पिछले सुख की स्मृति आँखों में
क्षण भर एक चमक है लाती,
तुरत शून्य में गड़ वह चितवन
तीखी नोंक सदृश बन जाती।
मानव की चेतना न ममता
रहती तब आँखों में उस क्षण!
हर्ष, शोक, अपमान, ग्लानि,
दुख दैन्य न जीवन का आकर्षण!
उस अवचेतन क्षण में मानो
वे सुदूर करतीं अवलोकन
ज्योति तमस के परदों पर
युग जीवन के पट का परिवर्तन!
अंधकार की अतल गुहा सी
अह, उन आँखों से डरता मन,
वर्ग सभ्यता के मंदिर के
निचले तल की वे वातायन!
वह बुड्ढा – सुमित्रानंदन पंत (12)
खड़ा द्वार पर, लाठी टेके,
वह जीवन का बूढ़ा पंजर,
चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी|
हिलते हड्डी के ढाँचे पर।
उभरी ढीली नसें जाल सी
सूखी ठठरी से हैं लिपटीं,
पतझर में ठूँठे तरु से ज्यों
सूनी अमरबेल हो चिपटी।
उसका लंबा डील डौल है,
हट्टी कट्टी काठी चौड़ी,
इस खँडहर में बिजली सी
उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी!
बैठी छाती की हड्डी अब,
झुकी रीढ़ कमटा सी टेढ़ी,
पिचका पेट, गढ़े कंधों पर,
फटी बिबाई से हैं एड़ी।
बैठे, टेक धरती पर माथा,
वह सलाम करता है झुककर,
उस धरती से पाँव उठा लेने को
जी करता है क्षण भर!
घुटनों से मुड़ उसकी लंबी
टाँगें जाँघें सटी परस्पर,
झुका बीच में शीश, झुर्रियों का
झाँझर मुख निकला बाहर।
हाथ जोड़, चौड़े पंजों की
गुँथी अँगुलियों को कर सन्मुख,
मौन त्रस्त चितवन से,
कातर वाणी से वह कहता निज दुख।
गर्मी के दिन, धरे उपरनी सिर पर,
लुंगी से ढाँपे तन,–
नंगी देह भरी बालों से,–
वन मानुस सा लगता वह जन।
भूखा है: पैसे पा, कुछ गुनमुना,
खड़ा हो, जाता वह धर,
पिछले पैरों के बल उठ
जैसे कोई चल रहा जानवर!
काली नारकीय छाया निज
छोड़ गया वह मेरे भीतर,
पैशाचिक सा कुछ: दुःखों से
मनुज गया शायद उसमें मर!
घंटा – सुमित्रानंदन पंत (13)
नभ की है उस नीली चुप्पी पर
घंटा है एक टंगा सुन्दर,
जो घड़ी घड़ी मन के भीतर
कुछ कहता रहता बज बज कर।
परियों के बच्चों से प्रियतर,
फैला कोमल ध्वनियों के पर
कानों के भीतर उतर उतर
घोंसला बनाते उसके स्वर।
भरते वे मन में मधुर रोर
जागो रे जागो, काम चोर!
डूबे प्रकाश में दिशा छोर
अब हुआ भोर, अब हुआ भोर!
आई सोने की नई प्रात:
कुछ नया काम हो, नई बात,
तुम रहो स्वच्छ मन, स्वच्छ गात,
निद्रा छोडो, रे गई, रात!
बापू – सुमित्रानंदन पंत (14)
चरमोन्नत जग में जब कि आज विज्ञान ज्ञान,
बहु भौतिक साधन, यंत्र यान, वैभव महान,
सेवक हैं विद्युत वाष्प शक्ति धन बल नितांत,
फिर क्यों जग में उत्पीड़न? जीवन यों अशांत?
मानव ने पाई देश काल पर जय निश्चय,
मानव के पास नहीं मानव का आज हृदय!
गर्वित उसका विज्ञान ज्ञान: वह नहीं पचित;
भौतिक मद से मानव आत्मा हो गई विजित!
है श्लाघ्य मनुज का भौतिक संचय का प्रयास,
मानवी भावना का क्या पर उसमें विकास?
चाहिये विश्व को आज भाव का नवोन्मेष,
मानव उर में फिर मानवता का हो प्रवेश!
बापू! तुम पर हैं आज लगे जग के लोचन,
तुम खोल नहीं जाओगे मानव के बंधन?
प्रथम रश्मि – सुमित्रानंदन पंत (15)
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि!
तूने कैसे पहचाना?
कहां, कहां हे बाल-विहंगिनि!
पाया तूने वह गाना?
सोयी थी तू स्वप्न नीड में,
पंखों के सुख में छिपकर,
ऊंघ रहे थे, घूम द्वार पर,
प्रहरी-से जुगनू नाना।
शशि-किरणों से उतर-उतरकर,
भू पर कामरूप नभ-चर,
चूम नवल कलियों का मृदु-मुख,
सिखा रहे थे मुसकाना।
स्नेह-हीन तारों के दीपक,
श्वास-शून्य थे तरु के पात,
विचर रहे थे स्वप्न अवनि में
तम ने था मंडप ताना।
कूक उठी सहसा तरु-वासिनि!
गा तू स्वागत का गाना,
किसने तुझको अंतर्यामिनि!
बतलाया उसका आना!
दो लड़के – सुमित्रानंदन पंत (16)
मेरे आँगन में, (टीले पर है मेरा घर)
दो छोटे-से लड़के आ जाते है अकसर!
नंगे तन, गदबदे, साँवले, सहज छबीले,
मिट्टी के मटमैले पुतले, – पर फुर्तीले।
जल्दी से टीले के नीचे उधर, उतरकर
वे चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुन्दर-
सिगरेट के ख़ाली डिब्बे, पन्नी चमकीली,
फीतों के टुकड़े, तस्वीरें नीली पीली
मासिक पत्रों के कवरों की, औ बन्दर से
किलकारी भरते हैं, खुश हो-हो अन्दर से।
दौड़ पार आँगन के फिर हो जाते ओझल
वे नाटे छः सात साल के लड़के मांसल
सुन्दर लगती नग्न देह, मोहती नयन-मन,
मानव के नाते उर में भरता अपनापन!
मानव के बालक है ये पासी के बच्चे
रोम-रोम मावन के साँचे में ढाले सच्चे!
अस्थि-मांस के इन जीवों की ही यह जग घर,
आत्मा का अधिवास न यह- वह सूक्ष्म, अनश्वर!
न्यौछावर है आत्मा नश्वर रक्त-मांस पर,
जग का अधिकारी है वह, जो है दुर्बलतर!
वह्नि, बाढ, उल्का, झंझा की भीषण भू पर
कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर?
निष्ठुर है जड़ प्रकृति, सहज भंगुर जीवित जन,
मानव को चाहिए जहाँ, मनुजोचित साधन!
क्यों न एक हों मानव-मानव सभी परस्पर
मानवता निर्माण करें जग में लोकोत्तर।
जीवन का प्रासाद उठे भू पर गौरवमय,
मानव का साम्राज्य बने, मानव-हित निश्चय।
दो लड़के – सुमित्रानंदन पंत (17)
मेरे आँगन में, (टीले पर है मेरा घर)
दो छोटे-से लड़के आ जाते है अकसर!
नंगे तन, गदबदे, साँवले, सहज छबीले,
मिट्टी के मटमैले पुतले, – पर फुर्तीले।
जल्दी से टीले के नीचे उधर, उतरकर
वे चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुन्दर-
सिगरेट के ख़ाली डिब्बे, पन्नी चमकीली,
फीतों के टुकड़े, तस्वीरें नीली पीली
मासिक पत्रों के कवरों की, औ बन्दर से
किलकारी भरते हैं, खुश हो-हो अन्दर से।
दौड़ पार आँगन के फिर हो जाते ओझल
वे नाटे छः सात साल के लड़के मांसल
सुन्दर लगती नग्न देह, मोहती नयन-मन,
मानव के नाते उर में भरता अपनापन!
मानव के बालक है ये पासी के बच्चे
रोम-रोम मावन के साँचे में ढाले सच्चे!
अस्थि-मांस के इन जीवों की ही यह जग घर,
आत्मा का अधिवास न यह- वह सूक्ष्म, अनश्वर!
न्यौछावर है आत्मा नश्वर रक्त-मांस पर,
जग का अधिकारी है वह, जो है दुर्बलतर!
वह्नि, बाढ, उल्का, झंझा की भीषण भू पर
कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर?
निष्ठुर है जड़ प्रकृति, सहज भंगुर जीवित जन,
मानव को चाहिए जहाँ, मनुजोचित साधन!
क्यों न एक हों मानव-मानव सभी परस्पर
मानवता निर्माण करें जग में लोकोत्तर।
जीवन का प्रासाद उठे भू पर गौरवमय,
मानव का साम्राज्य बने, मानव-हित निश्चय।
पर्वत प्रदेश में पावस – सुमित्रानंदन पंत (18)
पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश,
पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश।
मेखलाकर पर्वत अपार
अपने सहस्त्र दृग-सुमन फाड़,
अवलोक रहा है बार-बार
नीचे जल में निज महाकार,
-जिसके चरणों में पला ताल
दर्पण सा फैला है विशाल!
गिरि का गौरव गाकर झर-झर
मद में नस-नस उत्तेजित कर
मोती की लड़ियों सी सुन्दर
झरते हैं झाग भरे निर्झर!
गिरिवर के उर से उठ-उठ कर
उच्चाकांक्षायों से तरूवर
है झाँक रहे नीरव नभ पर
अनिमेष, अटल, कुछ चिंता पर।
उड़ गया, अचानक लो, भूधर
फड़का अपार वारिद के पर!
रव-शेष रह गए हैं निर्झर!
है टूट पड़ा भू पर अंबर!
धँस गए धरा में सभय शाल!
उठ रहा धुआँ, जल गया ताल
-यों जलद-यान में विचर-विचर
था इंद्र खेलता इंद्रजाल
विजय – सुमित्रानंदन पंत (19)
मैं चिर श्रद्धा लेकर आई
वह साध बनी प्रिय परिचय में,
मैं भक्ति हृदय में भर लाई,
वह प्रीति बनी उर परिणय में।
जिज्ञासा से था आकुल मन
वह मिटी, हुई कब तन्मय मैं,
विश्वास माँगती थी प्रतिक्षण
आधार पा गई निश्चय मैं !
प्राणों की तृष्णा हुई लीन
स्वप्नों के गोपन संचय में
संशय भय मोह विषाद हीन
लज्जा करुणा में निर्भय मैं !
लज्जा जाने कब बनी मान,
अधिकार मिला कब अनुनय में
पूजन आराधन बने गान
कैसे, कब? करती विस्मय मैं !
उर करुणा के हित था कातर
सम्मान पा गई अक्षय मैं,
पापों अभिशापों की थी घर
वरदान बनी मंगलमय मैं !
बाधा-विरोध अनुकूल बने
अंतर्चेतन अरुणोदय में,
पथ भूल विहँस मृदु फूल बने
मैं विजयी प्रिय, तेरी जय में।
लहरों का गीत – सुमित्रानंदन पंत (20)
अपने ही सुख से चिर चंचल
हम खिल खिल पडती हैं प्रतिपल,
जीवन के फेनिल मोती को
ले ले चल करतल में टलमल!
छू छू मृदु मलयानिल रह रह
करता प्राणों को पुलकाकुल;
जीवन की लतिका में लहलह
विकसा इच्छा के नव नव दल!
सुन मधुर मरुत मुरली की ध्वनि
गृह-पुलिन नांध, सुख से विह्वल,
हम हुलस नृत्य करतीं हिल हिल
खस खस पडता उर से अंचल!
चिर जन्म-मरण को हँस हँस कर
हम आलिंगन करती पल पल,
फिर फिर असीम से उठ उठ कर
फिर फिर उसमें हो हो ओझल!
यह धरती कितना देती है – सुमित्रानंदन पंत (21)
मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोये थे,
सोचा था, पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे,
रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी
और फूल फलकर मै मोटा सेठ बनूँगा!
पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा,
बन्ध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला!-
सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गये!
मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक
बाल-कल्पना के अपलक पाँवडे बिछाकर
मैं अबोध था, मैंने ग़लत बीज बोये थे,
ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था!
अर्द्धशती लहराती निकल गयी है तबसे!
कितने ही मधु पतझर बीत गये अनजाने,
ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, शरदें मुसकाई;
सी-सी कर हेमन्त कँपे, तरु झरे, खिले वन!
औ जब फिर से गाढ़ी, ऊदी लालसा लिये
गहरे, कजरारे बादल बरसे धरती पर,
मैंने कौतूहल-वश आँगन के कोने की
गीली तह यों ही उँगली से सहलाकर
बीज सेम के दबा दिये मिट्टी के नीचे-
भू के अंचल में मणि-माणिक बाँध दिये हो!
मैं फिर भूल गया इस छोटी-सी घटना को,
और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन!
किन्तु, एक दिन जब मैं सन्ध्या को आँगन में
टहल रहा था- तब सहसा, मैने देखा
उसे हर्ष-विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से!
देखा-आँगन के कोने में कई नवागत
छोटे-छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं!
छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ जीवन की,
या हथेलियाँ खोले थे वे नन्हीं प्यारी-
जो भी हो, वे हरे-हरे उल्लास से भरे
पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे-
डिम्ब तोड़कर निकले चिडियों के बच्चों से!
निर्निमेष, क्षण भर, मैं उनको रहा देखता-
सहसा मुझे स्मरण हो आया-कुछ दिन पहिले
बीज सेम के मैने रोपे थे आँगन में,
और उन्हीं से बौने पौधो की यह पलटन
मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से,
नन्हें नाटे पैर पटक, बढती जाती है!
तब से उनको रहा देखता धीरे-धीरे
अनगिनती पत्तों से लद, भर गयी झाड़ियाँ,
हरे-भरे टंग गये कई मखमली चँदोवे!
बेलें फैल गयी बल खा, आँगन में लहरा,
और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का
हरे-हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को-
मैं अवाक रह गया – वंश कैसे बढ़ता है!
छोटे तारों-से छितरे, फूलों के छीटें
झागों-से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर
सुन्दर लगते थे, मावस के हँसमुख नभ-से,
चोटी के मोती-से, आँचल के बूटों-से!
ओह, समय पर उनमें कितनी फलियाँ फूटी!
कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ-
पतली चौड़ी फलियाँ! उफ उनकी क्या गिनती!
लम्बी-लम्बी अँगुलियों – सी नन्हीं-नन्हीं
तलवारों-सी पन्ने के प्यारे हारों-सी,
झूठ न समझें चन्द्र कलाओं-सी नित बढ़ती,
सच्चे मोती की लड़ियों-सी, ढेर-ढेर खिल
झुण्ड-झुण्ड झिलमिलकर कचपचिया तारों-सी!
आह इतनी फलियाँ टूटी, जाड़ों भर खाईं,
सुबह शाम वे घर-घर पकीं, पड़ोस पास के
जाने-अनजाने सब लोगों में बँटव
बंधु-बांधवों, मित्रों, अभ्यागत, मँगतों ने
जी भर-भर दिन-रात महुल्ले भर ने खाईं !-
कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ!
यह धरती कितना देती है! धरती माता
कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को!
नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को,-
बचपन में छिः स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर!
रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ।
इसमें सच्ची समता के दाने बोने है;
इसमें जन की क्षमता का दाने बोने है,
इसमें मानव-ममता के दाने बोने हैं,-
जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें
मानवता की – जीवन श्रम से हँसे दिशाएँ-
हम जैसा बोयेंगे वैसा ही पायेंगे।
मैं सबसे छोटी होऊँ – सुमित्रानंदन पंत (22)
मैं सबसे छोटी होऊँ,
तेरी गोदी में सोऊँ,
तेरा अंचल पकड़-पकड़कर
फिरू सदा माँ! तेरे साथ,
कभी न छोड़ूँ तेरा हाथ!
बड़ा बनकर पहले हमको
तू पीछे चलती है मात!
हाथ पकड़ फिर सदा हमारे
साथ नहीं फिरती दिन-रात!
अपने कर से खिला, धुला मुख,
धूल पोंछ, सज्जित कर गात,
थमा खिलौने, नहीं सुनाती
हमें सुखद परियों की बात!
ऐसी बड़ी न होऊँ मैं
तेरा स्नेह न खोऊँ मैं,
तेरे अंचल की छाया में
छिपी रहूँ निस्पृह, निर्भय,
कहूँ-दिखा दे चंद्रोदय!
मछुए का गीत – सुमित्रानंदन पंत (23)
प्रेम की बंसी लगी न प्राण!
तू इस जीवन के पट भीतर
कौन छिपी मोहित निज छवि पर?
चंचल री नव यौवन के पर,
प्रखर प्रेम के बाण!
प्रेम की बंसी लगी न प्राण!
गेह लाड की लहरों का चल,
तज फेनिल ममता का अंचल,
अरी डूब उतरा मत प्रतिपल,
वृथा रूप का मान!
प्रेम की बंसी लगी न प्राण!
आए नव घन विविध वेश धर,
सुन री बहुमुख पावस के स्वर,
रूप वारी में लीन निरन्तर,
रह न सकेगी, मान!
प्रेम की बंसी लगी न प्राण!
नाव द्वार आवेगी बाहर,
स्वर्ण जाल में उलझ मनोहर,
बचा कौन जग में लुक छिप कर
बिंधते सब अनजान!
प्रेम की बंसी लगी न प्राण!
घिर घिर होते मेघ निछावर,
झर झर सर में मिलते निर्झर,
लिए डोर वह अंग जग की कर,
हरता तन मन प्राण!
प्रेम की बंसी लगी न प्राण!
चाँदनी – सुमित्रानंदन पंत (24)
नीले नभ के शतदल पर
वह बैठी शरद-हंसिनि,
मृदु-करतल पर शशि-मुख धर,
नीरव, अनिमिष, एकाकिनि!
वह स्वप्न-जड़ित नत-चितवन
छू लेती अंग-जग का मन,
श्यामल, कोमल, चल-चितवन
जो लहराती जग-जीवन!
वह फूली बेला की बन
जिसमें न नाल, दल, कुड्मल,
केवल विकास चिर-निर्मल
जिसमें डूबे दश दिशि-दल।
वह सोई सरित-पुलिन पर
साँसों में स्तब्ध समीरण,
केवल लघु-लघु लहरों पर
मिलता मृदु-मृदु उर-स्पन्दन।
अपनी छाया में छिपकर
वह खड़ी शिखर पर सुन्दर,
है नाच रहीं शत-शत छवि
सागर की लहर-लहर पर।
दिन की आभा दुलहिन बन
आई निशि-निभृत शयन पर,
वह छवि की छुईमुई-सी
मृदु मधुर-लाज से मर-मर।
जग के अस्फुट स्वप्नों का
वह हार गूँथती प्रतिपल,
चिर सजल-सजल, करुणा से
उसके ओसों का अंचल।
वह मृदु मुकुलों के मुख में
भरती मोती के चुम्बन,
लहरों के चल-करतल में
चाँदी के चंचल उडुगण।
वह लघु परिमल के घन-सी
जो लीन अनिल में अविकल,
सुख के उमड़े सागर-सी
जिसमें निमग्न उर-तट-स्थल।
वह स्वप्निल शयन-मुकुल-सी
हैं मुँदे दिवस के द्युति-दल,
उर में सोया जग का अलि,
नीरव जीवन-गुंजन कल!
वह नभ के स्नेह श्रवण में
दिशि का गोपन-सम्भाषण,
नयनों के मौन-मिलन में
प्राणों का मधुर समर्पण!
वह एक बूँद संसृति की
नभ के विशाल करतल पर,
डूबे असीम-सुखमा में
सब ओर-छोर के अन्तर।
झंकार विश्व-जीवन की
हौले हौले होती लय
वह शेष, भले ही अविदित,
वह शब्द-मुक्त शुचि-आशय।
वह एक अनन्त-प्रतीक्षा
नीरव, अनिमेष विलोचन,
अस्पृश्य, अदृश्य विभा वह,
जीवन की साश्रु-नयन क्षण।
वह शशि-किरणों से उतरी
चुपके मेरे आँगन पर,
उर की आभा में खोई,
अपनी ही छवि से सुन्दर।
वह खड़ी दृगों के सम्मुख
सब रूप, रेख रँग ओझल
अनुभूति-मात्र-सी उर में
आभास शान्त, शुचि, उज्ज्वल!
वह है, वह नहीं, अनिर्वच’,
जग उसमें, वह जग में लय,
साकार-चेतना सी वह,
जिसमें अचेत जीवाशय!
जीना अपने ही में – सुमित्रानंदन पंत (25)
जीना अपने ही में
एक महान कर्म है,
जीने का हो सदुपयोग
यह मनुज धर्म है।
अपने ही में रहना
एक प्रबुद्ध कला है,
जग के हित रहने में
सबका सहज भला है।
जग का प्यार मिले
जन्मों के पुण्य चाहिए,
जग जीवन को
प्रेम सिन्धु में डूब थाहिए।
ज्ञानी बनकर
मत नीरस उपदेश दीजिए,
लोक कर्म भव सत्य
प्रथम सत्कर्म कीजिए।
ग्राम श्री – सुमित्रानंदन पंत (26)
फैली खेतों में दूर तलक
मख़मल की कोमल हरियाली,
लिपटीं जिससे रवि की किरणें
चाँदी की सी उजली जाली !
तिनकों के हरे हरे तन पर
हिल हरित रुधिर है रहा झलक,
श्यामल भू तल पर झुका हुआ
नभ का चिर निर्मल नील फलक।
रोमांचित-सी लगती वसुधा
आयी जौ गेहूँ में बाली,
अरहर सनई की सोने की
किंकिणियाँ हैं शोभाशाली।
उड़ती भीनी तैलाक्त गन्ध,
फूली सरसों पीली-पीली,
लो, हरित धरा से झाँक रही
नीलम की कलि, तीसी नीली।
रँग रँग के फूलों में रिलमिल
हँस रही सखियाँ मटर खड़ी।
मख़मली पेटियों सी लटकीं
छीमियाँ, छिपाए बीज लड़ी।
फिरती हैं रँग रँग की तितली
रंग रंग के फूलों पर सुन्दर,
फूले फिरते हों फूल स्वयं
उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर।
अब रजत-स्वर्ण मंजरियों से
लद गईं आम्र तरु की डाली।
झर रहे ढाँक, पीपल के दल,
हो उठी कोकिला मतवाली।
महके कटहल, मुकुलित जामुन,
जंगल में झरबेरी झूली।
फूले आड़ू, नीबू, दाड़िम,
आलू, गोभी, बैंगन, मूली।
पीले मीठे अमरूदों में
अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ीं,
पक गये सुनहले मधुर बेर,
अँवली से तरु की डाल जड़ीं।
लहलह पालक, महमह धनिया,
लौकी औ सेम फली, फैलीं,
मख़मली टमाटर हुए लाल,
मिरचों की बड़ी हरी थैली।
गंजी को मार गया पाला,
अरहर के फूलों को झुलसा,
हाँका करती दिन भर बन्दर
अब मालिन की लड़की तुलसा।
बालाएँ गजरा काट-काट,
कुछ कह गुपचुप हँसतीं किन किन,
चाँदी की सी घंटियाँ तरल
बजती रहतीं रह रह खिन खिन।
छायातप के हिलकोरों में
चौड़ी हरीतिमा लहराती,
ईखों के खेतों पर सुफ़ेद
काँसों की झंड़ी फहराती।
ऊँची अरहर में लुका-छिपी
खेलतीं युवतियाँ मदमाती,
चुंबन पा प्रेमी युवकों के
श्रम से श्लथ जीवन बहलातीं।
बगिया के छोटे पेड़ों पर
सुन्दर लगते छोटे छाजन,
सुंदर, गेहूँ की बालों पर
मोती के दानों-से हिमकन।
प्रात: ओझल हो जाता जग,
भू पर आता ज्यों उतर गगन,
सुंदर लगते फिर कुहरे से
उठते-से खेत, बाग़, गृह, वन।
बालू के साँपों से अंकित
गंगा की सतरंगी रेती
सुंदर लगती सरपत छाई
तट पर तरबूज़ों की खेती।
अँगुली की कंघी से बगुले
कलँगी सँवारते हैं कोई,
तिरते जल में सुरख़ाब, पुलिन पर
मगरौठी रहती सोई।
डुबकियाँ लगाते सामुद्रिक,
धोतीं पीली चोंचें धोबिन,
उड़ अबालील, टिटहरी, बया,
चाहा चुगते कर्दम, कृमि, तृन।
नीले नभ में पीलों के दल
आतप में धीरे मँडराते,
रह रह काले, भूरे, सुफ़ेद
पंखों में रँग आते जाते।
लटके तरुओं पर विहग नीड़
वनचर लड़कों को हुए ज्ञात,
रेखा-छवि विरल टहनियों की
ठूँठे तरुओं के नग्न गात।
आँगन में दौड़ रहे पत्ते,
घूमती भँवर सी शिशिर वात।
बदली छँटने पर लगती प्रिय
ऋतुमती धरित्री सद्य स्नात।
हँसमुख हरियाली हिम-आतप
सुख से अलसाए-से सोये,
भीगी अँधियाली में निशि की
तारक स्वप्नों में-से-खोये,–
मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम–
जिस पर नीलम नभ आच्छादन,–
निरुपम हिमान्त में स्निग्ध शांत
निज शोभा से हरता जन मन!
याद – सुमित्रानंदन पंत (27)
विदा हो गई साँझ, विनत मुख पर झीना आँचल धर,
मेरे एकाकी आँगन में मौन मधुर स्मृतियाँ भर!
वह केसरी दुकूल अभी भी फहरा रहा क्षितिज पर,
नव असाढ़ के मेघों से घिर रहा बराबर अंबर!
मैं बरामदे में लेटा, शैय्या पर, पीड़ित अवयव,
मन का साथी बना बादलों का विषाद है नीरव!
सक्रिय यह सकरुण विषाद,–मेघों से उमड़ उमड़ कर
भावी के बहु स्वप्न, भाव बहु व्यथित कर रहे अंतर!
मुखर विरह दादुर पुकारता उत्कंठित भेकी को,
बर्हभार से मोर लुभाता मेघ-मुग्ध केकी को;
आलोकित हो उठता सुख से मेघों का नभ चंचल,
अंतरतम में एक मधुर स्मृति जग जग उठती प्रतिपल!
कम्पित करता वक्ष धरा का घन गंभीर गर्जन स्वर,
भू पर ही आगया उतर शत धाराओं में अंबर!
भीनी भीनी भाप सहज ही साँसों में घुल मिल कर
एक और भी मधुर गंध से हृदय दे रही है भर!
नव असाढ़ की संध्या में, मेघों के तम में कोमल,
पीड़ित एकाकी शय्या पर, शत भावों से विह्वल,
एक मधुरतम स्मृति पल भर विद्युत सी जल कर उज्वल
याद दिलाती मुझे हृदय में रहती जो तुम निश्चल!
चींटी – सुमित्रानंदन पंत (28)
चींटी को देखा?
वह सरल, विरल, काली रेखा,
तम के तागे सी जो हिल-डुल,
चलती लघु पद पल-पल मिल-जुल,
यह है पिपीलिका पाँति! देखो ना, किस भाँति,
काम करती वह सतत, कन-कन कनके चुनती अविरत।
गाय चराती, धूप खिलाती,
बच्चों की निगरानी करती,
लड़ती, अरि से तनिक न डरती,
दल के दल सेना संवारती,
घर-आँगन, जनपथ बुहारती।
चींटी है प्राणी सामाजिक,
वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक।
देखा चींटी को?
उसके जी को?
भूरे बालों की सी कतरन,
छुपा नहीं उसका छोटापन,
वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर,
विचरण करती, श्रम में तन्मय,
वह जीवन की तिनगी अक्षय।
वह भी क्या देही है, तिल-सी?
प्राणों की रिलमिल झिलमिल-सी।
दिनभर में वह मीलों चलती,
अथक कार्य से कभी न टलती।
ताज – सुमित्रानंदन पंत (29)
हाय! मृत्यु का ऐसा अमर, अपार्थिव पूजन?
जब निषण्ण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन!
संग-सौध में हो शृंगार मरण का शोभन,
नग्न, क्षुधातुर, वास-विहीन रहें जीवित जन?
मानव! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति?
आत्मा का अपमान, प्रेत औ’ छाया से रति!!
प्रेम-अर्चना यही, करें हम मरण को वरण?
स्थापित कर कंकाल, भरें जीवन का प्रांगण?
शव को दें हम रूप, रंग, आदर मानव का
मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का?
गत-युग के बहु धर्म-रूढ़ि के ताज मनोहर
मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर!
भूल गये हम जीवन का संदेश अनश्वर,
मृतकों के हैं मृतक, जीवतों का है ईश्वर!
बाल प्रश्न – सुमित्रानंदन पंत (30)
माँ! अल्मोड़े में आए थे
जब राजर्षि विवेकानंदं,
तब मग में मखमल बिछवाया,
दीपावली की विपुल अमंद,
बिना पाँवड़े पथ में क्या वे
जननि! नहीं चल सकते हैं?
दीपावली क्यों की? क्या वे माँ!
मंद दृष्टि कुछ रखते हैं?
कृष्ण! स्वामी जी तो दुर्गम
मग में चलते हैं निर्भय,
दिव्य दृष्टि हैं, कितने ही पथ
पार कर चुके कंटकमय,
वह मखमल तो भक्तिभाव थे
फैले जनता के मन के,
स्वामी जी तो प्रभावान हैं
वे प्रदीप थे पूजन के।
धरती का आँगन इठलाता – सुमित्रानंदन पंत (31)
धरती का आँगन इठलाता!
शस्य श्यामला भू का यौवन
अंतरिक्ष का हृदय लुभाता!
जौ गेहूँ की स्वर्णिम बाली
भू का अंचल वैभवशाली
इस अंचल से चिर अनादि से
अंतरंग मानव का नाता!
आओ नए बीज हम बोएं
विगत युगों के बंधन खोएं
भारत की आत्मा का गौरव
स्वर्ग लोग में भी न समाता!
भारत जन रे धरती की निधि,
न्यौछावर उन पर सहृदय विधि,
दाता वे, सर्वस्व दान कर
उनका अंतर नहीं अघाता!
किया उन्होंने त्याग तप वरण,
जन स्वभाव का स्नेह संचरण
आस्था ईश्वर के प्रति अक्षय
श्रम ही उनका भाग्य विधाता!
सृजन स्वभाव से हो उर प्रेरित
नव श्री शोभा से उन्मेषित
हम वसुधैव कुटुम्ब ध्येय रख
बनें नये युग के निर्माता!
आत्मा का चिर-धन – सुमित्रानंदन पंत (32)
क्या मेरी आत्मा का चिर-धन ?
मैं रहता नित उन्मन, उन्मन!
प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर,
त्रिण, तरु, पशु, पक्षी, नर, सुरवर,
सुन्दर अनादि शुभ सृष्टि अमर;
निज सुख से ही चिर चंचल-मन,
मैं हूँ प्रतिपल उन्मन, उन्मन।
मैं प्रेमी उच्चादर्शों का,
संस्कृति के स्वर्गिक-स्पर्शो का,
जीवन के हर्ष-विमर्शों का,
लगता अपूर्ण मानव जीवन,
मैं इच्छा से उन्मन, उन्मन!
जग-जीवन में उल्लास मुझे,
नव-आशा, नव अभिलाष मुझे,
ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे;
चाहिए विश्व को नवजीवन,
मैं आकुल रे उन्मन, उन्मन।
भारतमाता – सुमित्रानंदन पंत (33)
भारत माता
ग्रामवासिनी।
खेतों में फैला है श्यामल
धूल भरा मैला सा आँचल,
गंगा यमुना में आँसू जल,
मिट्टी कि प्रतिमा
उदासिनी।
दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन,
अधरों में चिर नीरव रोदन,
युग युग के तम से विषण्ण मन,
वह अपने घर में
प्रवासिनी।
तीस कोटि संतान नग्न तन,
अर्ध क्षुधित, शोषित, निरस्त्र जन,
मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन,
नत मस्तक
तरु तल निवासिनी!
स्वर्ण शस्य पर -पदतल लुंठित,
धरती सा सहिष्णु मन कुंठित,
क्रन्दन कंपित अधर मौन स्मित,
राहु ग्रसित
शरदेन्दु हासिनी।
चिन्तित भृकुटि क्षितिज तिमिरांकित,
नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित,
आनन श्री छाया-शशि उपमित,
ज्ञान मूढ़
गीता प्रकाशिनी!
सफल आज उसका तप संयम,
पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम,
हरती जन मन भय, भव तम भ्रम,
जग जननी
जीवन विकासिनी।
नौका-विहार – सुमित्रानंदन पंत (34)
शांत स्निग्ध, ज्योत्स्ना उज्ज्वल!
अपलक अनंत, नीरव भू-तल!
सैकत-शय्या पर दुग्ध-धवल, तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म-विरल,
लेटी हैं श्रान्त, क्लान्त, निश्चल!
तापस-बाला गंगा, निर्मल, शशि-मुख से दीपित मृदु-करतल,
लहरे उर पर कोमल कुंतल।
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुन्दर
चंचल अंचल-सा नीलांबर!
साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर, शशि की रेशमी-विभा से भर,
सिमटी हैं वर्तुल, मृदुल लहर।
चाँदनी रात का प्रथम प्रहर,
हम चले नाव लेकर सत्वर।
सिकता की सस्मित-सीपी पर, मोती की ज्योत्स्ना रही विचर,
लो, पालें चढ़ीं, उठा लंगर।
मृदु मंद-मंद, मंथर-मंथर, लघु तरणि, हंसिनी-सी सुन्दर
तिर रही, खोल पालों के पर।
निश्चल-जल के शुचि-दर्पण पर, बिम्बित हो रजत-पुलिन निर्भर
दुहरे ऊँचे लगते क्षण भर।
कालाकाँकर का राज-भवन, सोया जल में निश्चिंत, प्रमन,
पलकों में वैभव-स्वप्न सघन।
नौका से उठतीं जल-हिलोर,
हिल पड़ते नभ के ओर-छोर।
विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल
ज्योतित कर नभ का अंतस्तल,
जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किये अविरल
फिरतीं लहरें लुक-छिप पल-पल।
सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी-सी जल में कल,
रुपहरे कचों में ही ओझल।
लहरों के घूँघट से झुक-झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक्-मुख
दिखलाता, मुग्धा-सा रुक-रुक।
अब पहुँची चपला बीच धार,
छिप गया चाँदनी का कगार।
दो बाहों-से दूरस्थ-तीर, धारा का कृश कोमल शरीर
आलिंगन करने को अधीर।
अति दूर, क्षितिज पर विटप-माल, लगती भ्रू-रेखा-सी अराल,
अपलक-नभ नील-नयन विशाल;
मा के उर पर शिशु-सा, समीप, सोया धारा में एक द्वीप,
ऊर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप;
वह कौन विहग? क्या विकल कोक, उड़ता, हरने का निज विरह-शोक?
छाया की कोकी को विलोक?
पतवार घुमा, अब प्रतनु-भार,
नौका घूमी विपरीत-धार।
ड़ाँड़ों के चल करतल पसार, भर-भर मुक्ताफल फेन-स्फार,
बिखराती जल में तार-हार।
चाँदी के साँपों-सी रलमल, नाँचतीं रश्मियाँ जल में चल
रेखाओं-सी खिंच तरल-सरल।
लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ-सौ शशि, सौ-सौ उडु झिलमिल
फैले फूले जल में फेनिल।
अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले-ले सहज थाह
हम बढ़े घाट को सहोत्साह।
ज्यों-ज्यों लगती है नाव पार
उर में आलोकित शत विचार।
इस धारा-सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम,
शाश्वत है गति, शाश्वत संगम।
शाश्वत नभ का नीला-विकास, शाश्वत शशि का यह रजत-हास,
शाश्वत लघु-लहरों का विलास।
हे जग-जीवन के कर्णधार! चिर जन्म-मरण के आर-पार,
शाश्वत जीवन-नौका-विहार।
मै भूल गया अस्तित्व-ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण
करता मुझको अमरत्व-दान।
पाषाण खंड – सुमित्रानंदन पंत (35)
वह अनगढ़ पाषाण खंड था-
मैंने तपकर, खंटकर,
भीतर कहीं सिमटकर
उसका रूप निखारा
तदवत भाव उतारा
श्री मुख का
सौंदर्य सँवारा!
लोग उसे
निज मुख बतलाते
देख-देख कर नहीं अघाते
वह तो प्रेम
तुम्हारा प्रिय मुख
तन्मय अंतर को
देता सुख।
जग-जीवन में जो चिर महान – सुमित्रानंदन पंत (36)
जग-जीवन में जो चिर महान,
सौंदर्य – पूर्ण औ सत्य – प्राण,
मैं उसका प्रेमी बनूँ, नाथ!
जिसमें मानव – हित हो समान!
जिससे जीवन में मिले शक्ति,
छूटें भय, संशय, अंध – भक्ति;
मैं वह प्रकाश बन सकूँ, नाथ!
मिज जावें जिसमें अखिल व्यक्ति!
दिशि-दिशि में प्रेम – प्रभा प्रसार,
हर भेद – भाव का अंधकार,
मैं खोल सकूँ चिर मुँदे, नाथ!
मानव के उर के स्वर्ग-द्वार!
पाकर, प्रभु! तुमसे अमर दान
करने मानव का परित्राण,
ला सकूँ विश्व में एक बार
फिर से नव जीवन का विहान!
परिवर्तन – सुमित्रानंदन पंत (37)
(1)
आज कहां वह पूर्ण-पुरातन, वह सुवर्ण का काल?
भूतियों का दिगंत-छवि-जाल,
ज्योति-चुम्बित जगती का भाल?
राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन-विस्तार?
स्वर्ग की सुषमा जब साभार
धरा पर करती थी अभिसार!
प्रसूनों के शाश्वत-शृंगार,
(स्वर्ण-भृंगों के गंध-विहार)
गूंज उठते थे बारंबार,
सृष्टि के प्रथमोद्गार!
नग्न-सुंदरता थी सुकुमार,
ॠध्दि औ’ सिध्दि अपार!
अये, विश्व का स्वर्ण-स्वप्न, संसृति का प्रथम-प्रभात,
कहाँ वह सत्य, वेद-विख्यात?
दुरित, दु:ख, दैन्य न थे जब ज्ञात,
अपरिचित जरा-मरण-भ्रू-पात!
(2)
अहे निष्ठुर परिवर्तन!
तुम्हारा ही तांडव नर्तन
विश्व का करुण विवर्तन!
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन
निखिल उत्थान, पतन!
अहे वासुकि सहस्र फन!
छोड़ द्रुमों की मृदु छाया – सुमित्रानंदन पंत (38)
छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले! तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन?
भूल अभी से इस जग को!
तज कर तरल तरंगों को,
इन्द्रधनुष के रंगों को,
तेरे भ्रू भ्रंगों से कैसे बिधवा दूँ निज मृग सा मन?
भूल अभी से इस जग को!
कोयल का वह कोमल बोल,
मधुकर की वीणा अनमोल,
कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूँ, सजनि, श्रवण?
भूल अभी से इस जग को!
ऊषा-सस्मित किसलय-दल,
सुधा-रश्मि से उतरा जल,
ना, अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूँ जीवन?
भूल अभी से इस जग को!
धेनुएँ – सुमित्रानंदन पंत (39)
ओ रंभाती नदियों,
बेसुध
कहाँ भागी जाती हो?
वंशी-रव
तुम्हारे ही भीतर है!
ओ, फेन-गुच्छ
लहरों की पूँछ उठाए
दौड़ती नदियों,
इस पार उस पार भी देखो,
जहाँ फूलों के कूल
सुनहरे धान से खेत हैं।
कल-कल छल-छल
अपनी ही विरह व्यथा
प्रीति कथा कहती
मत चली जाओ!
सागर ही तुम्हारा सत्य नहीं
वह तो गतिमय स्त्रोत की तरह
पन्द्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस – सुमित्रानंदन पंत (40)
चिर प्रणम्य यह पुष्य अहन, जय गाओ सुरगण,
आज अवतरित हुई चेतना भू पर नूतन !
नव भारत, फिर चीर युगों का तिमिर-आवरण,
तरुण अरुण-सा उदित हुआ परिदीप्त कर भुवन !
सभ्य हुआ अब विश्व, सभ्य धरणी का जीवन,
आज खुले भारत के संग भू के जड़-बंधन !
शान्त हुआ अब युग-युग का भौतिक संघर्षण,
मुक्त चेतना भारत की यह करती घोषण !
आम्र-मौर लाओ हे ,कदली स्तम्भ बनाओ,
पावन गंगा जल भर के बंदनवार बँधाओ,
जय भारत गाओ, स्वतन्त्र भारत गाओ !
उन्नत लगता चन्द्र कला स्मित आज हिमाँचल,
चिर समाधि से जाग उठे हों शम्भु तपोज्वल !
लहर-लहर पर इन्द्रधनुष ध्वज फहरा चंचल
जय निनाद करता, उठ सागर, सुख से विह्वल !
धन्य आज का मुक्ति-दिवस गाओ जन-मंगल,
भारत लक्ष्मी से शोभित फिर भारत शतदल !
तुमुल जयध्वनि करो महात्मा गान्धी की जय
नव भारत के सुज्ञ सारथी वह नि:संशय !
राष्ट्र-नायकों का हे, पुन: करो अभिवादन,
जीर्ण जाति में भरा जिन्होंने नूतन जीवन !
स्वर्ण-शस्य बाँधो भू वेणी में युवती जन,
बनो वज्र प्राचीर राष्ट्र की, वीर युवगण!
लोह-संगठित बने लोक भारत का जीवन,
हों शिक्षित सम्पन्न क्षुधातुर नग्न-भग्न जन!
मुक्ति नहीं पलती दृग-जल से हो अभिसिंचित,
संयम तप के रक्त-स्वेद से होती पोषित!
मुक्ति माँगती कर्म वचन मन प्राण समर्पण,
वृद्ध राष्ट्र को, वीर युवकगण, दो निज यौवन!
नव स्वतंत्र भारत, हो जग-हित ज्योति जागरण,
नव प्रभात में स्वर्ण-स्नात हो भू का प्रांगण !
नव जीवन का वैभव जाग्रत हो जनगण में,
आत्मा का ऐश्वर्य अवतरित मानव मन में!
रक्त-सिक्त धरणी का हो दु:स्वप्न समापन,
शान्ति प्रीति सुख का भू-स्वर्ग उठे सुर मोहन!
भारत का दासत्व दासता थी भू-मन की,
विकसित आज हुई सीमाएँ जग-जीवन की!
धन्य आज का स्वर्ण दिवस, नव लोक-जागरण!
नव संस्कृति आलोक करे, जन भारत वितरण!
नव-जीवन की ज्वाला से दीपित हों दिशि क्षण,
नव मानवता में मुकुलित धरती का जीवन !
गीत विहग – सुमित्रानंदन पंत (41)
ये गीत विहग उड़-उड़ जाते !
भावों के पंख लगे सुन्दर,
सपनों से रच संसार सुघर,
भरते उड़ान नभ को छूते
मेरे मन भीतर सुख पाते !
चमकीली रंगभरी आँखें,
रंगों में डूबी हैं पाँखें,
अपना नन्हा-सा कंठ खोल
मेरे स्वर में स्वर भर गाते !
खिल गया फूल जब तुम बोले,
कलियों ने भी घूँघट खोले,
भँवरा मधु पी चुपचाप रहा
तुम स्वर में मधु-रस भर लाते !
तुम धवल बनो हिम शिखरों-सा
गंभीर बनो जैसा सागर !
सहते जाओ जैसे अवनी
उड़ चलो परों को फहराते !
तुम साँस-साँस में गंध भरो,
जीवन का सब दु:ख शोक हरो,
अमृत बन जाये मरण तभी
जब तुम इन प्राणों में छाते !
ये गीत विहग उड़-उड़ जाते !
जग के उर्वर आँगन में – सुमित्रानंदन पंत (42)
जग के उर्वर – आँगन में
बरसो ज्योतिर्मय जीवन!
बरसो लघु – लघु तृण, तरु पर
हे चिर – अव्यय, चिर – नूतन!
बरसो कुसुमों में मधु बन,
प्राणों में अमर प्रणय – धन;
स्मिति – स्वप्न अधर – पलकों में,
उर-अंगों में सुख-यौवन!
छू-छू जग के मृत रज – कण
कर दो तृण – तरु में चेतन,
मृन्मरण बाँध दो जग का,
दे प्राणों का आलिंगन!
बरसो सुख बन, सुखमा बन,
बरसो जग – जीवन के घन!
दिशि – दिशि में औ’ पल – पल में
बरसो संसृति के सावन!
काले बादल – सुमित्रानंदन पंत (43)
सुनता हूँ, मैंने भी देखा,
काले बादल में रहती चाँदी की रेखा!
काले बादल जाति द्वेष के,
काले बादल विश्व क्लेश के,
काले बादल उठते पथ पर
नव स्वतंत्रता के प्रवेश के!
सुनता आया हूँ, है देखा,
काले बादल में हँसती चाँदी की रेखा!
आज दिशा हैं घोर अँधेरी
नभ में गरज रही रण भेरी,
चमक रही चपला क्षण-क्षण पर
झनक रही झिल्ली झन-झन कर!
नाच-नाच आँगन में गाते केकी-केका
काले बादल में लहरी चाँदी की रेखा।
काले बादल, काले बादल,
मन भय से हो उठता चंचल!
कौन हृदय में कहता पलपल
मृत्यु आ रही साजे दलबल!
आग लग रही, घात चल रहे, विधि का लेखा!
काले बादल में छिपती चाँदी की रेखा!
मुझे मृत्यु की भीति नहीं है,
पर अनीति से प्रीति नहीं है,
यह मनुजोचित रीति नहीं है,
जन में प्रीति प्रतीति नहीं है!
देश जातियों का कब होगा,
नव मानवता में रे एका,
काले बादल में कल की,
सोने की रेखा!
तप रे! – सुमित्रानंदन पंत (44)
तप रे, मधुर मन!
विश्व-वेदना में तप प्रतिपल,
जग-जीवन की ज्वाला में गल,
बन अकलुष, उज्ज्वल और कोमल
तप रे, विधुर-विधुर मन!
अपने सजल-स्वर्ण से पावन
रच जीवन की पूर्ति पूर्णतम
स्थापित कर जग अपनापन,
ढल रे, ढल आतुर मन!
तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन,
गंध-हीन तू गंध-युक्त बन,
निज अरूप में भर स्वरूप, मन
मूर्तिमान बन निर्धन!
गल रे, गल निष्ठुर मन!
आजाद – सुमित्रानंदन पंत (45)
पैगम्बर के एक शिष्य ने
पूछा, हजरत बंदे को शक
है आज़ाद कहां तक इंसा
दुनिया में, पाबंद कहां तक?
खड़े रहो! बोले रसूल तब,
अच्छा, पैर उठाओ ऊपर
जैसा हुक्म! मुरीद सामने
खड़ा हो गया एक पैर पर!
ठीक , दूसरा पैर उठाओ
बोले हंस कर नबी फिर तुरंत,
बार बार गिर, कहा शिष्य ने
यह तो नामुमकिन है हजरत
हो आज़ाद यहां तक, कहता
तुमसे एक पैर उठ उपर,
बंधे हुए दुनिया से, कहता
पैर दूसरा अड़ा जमीं पर! –
पैगम्बर का था यह उत्तर!
द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र – सुमित्रानंदन पंत (46)
द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र!
हे स्रस्त-ध्वस्त! हे शुष्क-शीर्ण!
हिम-ताप-पीत, मधुवात-भीत,
तुम वीत-राग, जड़, पुराचीन!!
निष्प्राण विगत-युग! मृतविहंग!
जग-नीड़, शब्द औ श्वास-हीन,
च्युत, अस्त-व्यस्त पंखों-से तुम
झर-झर अनन्त में हो विलीन!
कंकाल-जाल जग में फैले
फिर नवल रुधिर,-पल्लव-लाली!
प्राणों की मर्मर से मुखरित
जीव की मांसल हरियाली!
मंजरित विश्व में यौवन के
जग कर जग का पिक, मतवाली
निज अमर प्रणय-स्वर मदिरा से
भर दे फिर नव-युग की प्याली!
गंगा – सुमित्रानंदन पंत (47)
अब आधा जल निश्चल, पीला,–
आधा जल चंचल औ’, नीला–
गीले तन पर मृदु संध्यातप
सिमटा रेशम पट सा ढीला।
ऐसे सोने के साँझ प्रात:,
ऐसे चाँदी के दिवस रात,
ले जाती बहा कहाँ गंगा
जीवन के युग क्षण,– किसे ज्ञात!
विश्रुत हिम पर्वत से निर्गत,
किरणोज्वल चल कल ऊर्मि निरत,
यमुना, गोमती आदि से मिल
होती यह सागर में परिणत।
यह भौगोलिक गंगा परिचित,
जिसके तट पर बहु नगर प्रथित,
इस जड़ गंगा से मिली हुई
जन गंगा एक और जीवित!
वह विष्णुपदी, शिव मौलि स्रुता,
वह भीष्म प्रसू औ’ जह्नु सुता,
वह देव निम्नगा, स्वर्ग गंगा,
वह सगर पुत्र तारिणी श्रुता।
वह गंगा, यह केवल छाया,
वह लोक चेतना, यह माया,
वह आत्म वाहिनी ज्योति सरी,
यह भू पतिता, कंचुक काया।
वह गंगा जन मन से नि:सृत,
जिसमें बहु बुदबुद युग नर्तित,
वह आज तरंगित, संसृति के
मृत सैकत को करने प्लावित।
दिशि दिशि का जन मत वाहित कर,
वह बनी अकूल अतल सागर,
भर देगी दिशि पल पुलिनों में
वह नव नव जीवन की मृद उर्वर!
अब नभ पर रेखा शशि शोभित,
गंगा का जल श्यामल, कम्पित,
लहरों पर चाँदी की किरणें
करतीं प्रकाशमय कुछ अंकित!
अमर स्पर्श – सुमित्रानंदन पंत (48)
खिल उठा हृदय,
पा स्पर्श तुम्हारा अमृत अभय!
खुल गए साधना के बंधन,
संगीत बना, उर का रोदन,
अब प्रीति द्रवित प्राणों का पण,
सीमाएँ अमिट हुईं सब लय।
क्यों रहे न जीवन में सुख दुख,
क्यों जन्म मृत्यु से चित्त विमुख?
तुम रहो दृगों के जो सम्मुख,
प्रिय हो मुझको भ्रम भय संशय!
तन में आएँ शैशव यौवन,
मन में हों विरह मिलन के व्रण,
युग स्थितियों से प्रेरित जीवन,
उर रहे प्रीति में चिर तन्मय!
जो नित्य अनित्य जगत का क्रम,
वह रहे, न कुछ बदले, हो कम,
हो प्रगति ह्रास का भी विभ्रम,
जग से परिचय, तुमसे परिणय!
तुम सुंदर से बन अति सुंदर,
आओ अंतर में अंतर तर,
तुम विजयी जो, प्रिय हो मुझ पर
वरदान, पराजय हो निश्चय!
आओ, हम अपना मन टोवें – सुमित्रानंदन पंत (49)
आओ, अपने मन को टोवें!
व्यर्थ देह के सँग मन की भी,
निर्धनता का बोझ न ढोवें।
जाति पाँतियों में बहु बट कर,
सामाजिक जीवन संकट वर,
स्वार्थ लिप्त रह, सर्व श्रेय के,
पथ में हम मत काँटे बोवें!
उजड़ गया घर द्वार अचानक,
रहा भाग्य का खेल भयानक,
बीत गयी जो बीत गयी, हम,
उसके लिये नहीं अब रोवें!
परिवर्तन ही जग का जीवन,
यहाँ विकास ह्रास संग विघटन,
हम हों अपने भाग्य विधाता,
यों मन का धीरज मत खोवें!
साहस, दृढ संकल्प, शक्ति, श्रम,
नवयुग जीवन का रच उपक्रम,
नव आशा से नव आस्था से,
नए भविष्यत स्वप्न सजोवें!
नया क्षितिज अब खुलता मन में,
नवोन्मेष जन-भू जीवन में,
राग द्वेष के, प्रकृति विकृति के,
युग युग के घावों को धोवें!
कुछ प्रसिद्ध कविताएँ :-
- रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध कविताएं
- हरिवंश राय बच्चन के प्रसिद्ध कविताएं
- माखन लाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध कविताएं
- रहिमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाय
- सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ के प्रसिद्ध कविताएँ
- संत कबीर दास जी के प्रसिद्ध दोहे अर्थ सहित
- सूरदास के प्रसिद्ध कविताएँ
- सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रसिद्ध कविताएँ
- महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध कविताएँ
- जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध कविताएं
- मैथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध कविताएं
- मैथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध कविताएं